(विकास मिश्र)
‘शिव और शक्ति’ ये दो नाम मात्र प्रतीक हैं उस अनादि, अनन्त, अपौरुषेय तत्त्व के, जो स्वयं में पूर्ण है और जिसकी महिमा से समस्त सृष्टि का प्रारंभ, संचालन और संहार होता है। ‘शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं’ यह श्लोक शृंगारलहरी का प्रथम श्लोक है, इसका तात्त्विक मर्म अत्यंत गम्भीर है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब तक शिव शक्ति से युक्त नहीं होते, वे न तो कोई कार्य कर सकते हैं और न ही कोई गति उनमें संभव है। उनका हिलना-डुलना भी शक्ति के बिना असंभव है। यह अभिव्यक्ति अध्यात्म की मूल चेतना है कि ऊर्जा और चेतना का यह सह-अस्तित्व ही ब्रह्माण्डीय समरसता का आधार है।
शिव यदि निर्विकार सत्ता हैं तो शक्ति उसी सत्ता की विकारी अभिव्यक्ति है। शिव यदि कूटस्थ, निश्चल, अचल आत्मा है तो शक्ति वह गति है, जो शब्दरूप ब्रह्मांडों में प्रतिक्षण प्रकट हो रही है। शक्ति वह लहर है जो शिव के सागर में उत्पन्न होती है और पुनः उसी में विलीन हो जाती है। शिव ज्यों निर्विकल्प शून्यता है, वहीं शक्ति विकल्पमयी पूर्णता है।
शिव अद्वैत का प्रतीक है तो शक्ति द्वैत का आरंभ; और दोनों के मेल से ही वह लयात्मक समन्वय उत्पन्न होता है, जिसे हम जीवन कहते हैं। यह जीवन सृष्टि, स्थिति और लय की त्रयी में उसी प्रकार प्रवाहित होता है, जैसे ओंकार के तीन मात्राएँ— अ, उ, म; अंततः एक ही मौन में विलीन हो जाती हैं।
यद्यपि शिव उस चेतना के रूप हैं, जो स्वयं में स्थित है, जो नित्य है, अजर है, अक्लिष्ट है और अचल है। वह आत्मस्वरूप ब्रह्म है, जिसे ‘सत्-चित्-आनन्द’ कहा गया है। वहीं शक्ति उस आत्मस्वरूप का बाह्य प्रकटीकरण है जो नाम-रूप से युक्त, क्रियाशील, सगुण, प्रकट, दृश्य एवं संवेदनशील। यह शक्ति ही प्रकृति है, यह माया है, यह वही चित्शक्ति है जो शिव की निष्क्रियता को कर्म में परिणत करती है। यह वही दिव्य स्त्रीतत्त्व है, जो पुरुष के मौन में अर्थ भरती है, उसकी निष्क्रिय सत्ता को गति देती है।
इस तात्त्विक भेद के माध्यम से जब हम आत्मबोध की ओर अग्रसर होते हैं, तो ज्ञात होता है कि यह भेद भी केवल प्रतीतिमात्र है। वास्तव में शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। शक्ति के बिना शिव शववत् हैं और शिव के बिना शक्ति केवल व्यर्थ चपलता है। इन दोनों के अभिन्न भाव को जो जानता है, वही ब्रह्म को जानता है। यही वह द्वैताभास में अद्वैत का रहस्य है, जो उपनिषदों से लेकर तांत्रिक ग्रंथों तक, योग से लेकर वेदांत तक प्रतिपादित होता रहा है।
मानव जीवन के धरातल पर शिव और शक्ति की यह एकता साधना का विषय बन जाती है। साधक जब तक केवल शक्ति में आसक्त रहता है, तब तक वह चंचलता, विक्षोभ और परिवर्तन के जाल में उलझा रहता है। जब वह शिवत्व का साक्षात्कार करता है, तब वह स्थिरता, शान्ति और ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है। किन्तु जब वह जानता है कि शक्ति और शिव एक ही तत्त्व के दो पक्ष हैं- एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही दीपक की लौ और प्रकाश तब उसका साधकत्व पूर्णता को प्राप्त करता है। यही पूर्णता ही मोक्ष है, यही आत्मबोध है, यही शिवत्व की सिद्धि है।
अतः अहंकार, देहबुद्धि और आत्मभ्रम की जो परतें व्यक्ति के आत्मचेतना को आवरित किए रहती हैं, वे शक्ति की ओर से ही निर्मित होती हैं, किंतु उसी शक्ति की साधना के माध्यम से, उसी प्रकृति की राह से जब साधक आगे बढ़ता है और अंततः उसे पार करता है, तब वह शिव का अनुभव करता है। यही शक्ति का उपदेश है कि वह स्वयं ही मार्ग है और स्वयं ही लक्ष्य का द्वार भी। शिव को पाने का मार्ग शक्ति से होकर ही जाता है और शक्ति को जानने के लिए शिव में स्थिर होना पड़ता है। यही द्विविध साधना की एकरूप परिणति है।
शिवशक्ति की यह एकता वैदिक ऋषियों की वाणी में भी व्याप्त है ‘ईशावास्यमिदं सर्वं’ यह सर्वथा शिवमयी सत्ता है। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है, वह उसी एक आत्मा की अनेक शक्तियों की लीलामयी प्रतिच्छाया है। शक्ति जब तमोमयी होती है, तो वह मोह और बंधन का कारण बनती है। जब वह सत्त्वगुणी होती है, तब वह ध्यान, ज्ञान और मोक्ष का द्वार खोलती है। और जब वह समत्व को प्राप्त करती है, तब वह शिवस्वरूप में विलीन हो जाती है। यही लय, यही संयोग, यही महायोग है।
शिव के सन्दर्भ में जो ‘स्थाणु’ है वह अचल, अपरिवर्तनीय, अजर और अमर वहीं शक्ति की अभिव्यक्ति नृत्य है, ‘नटराज’ के उस चिदम्बर नृत्य में जहाँ प्रत्येक थिरकन, प्रत्येक कंपन में ब्रह्म की रचना, पालन और संहार की लय है। वह नृत्य केवल एक दृश्य क्रिया नहीं, वह स्वयं ब्रह्म का ध्वनि में रूपांतरण है। उसमें ताण्डव भी है और लास्य भी। एक ही नाद में महाविनाश और महासृजन दोनों समाहित हैं। वह चित्त की अपूर्व एकाग्रता है, जहाँ चित्त ही शक्ति हो जाती है और शक्ति ही शिव में विलीन हो जाती है। जब योग के माध्यम से साधक अपने चित्त को शुद्ध करता है, तो उस चित्त की शुद्धता ही अंततः शक्ति की शुद्धता बन जाती है।
जैसे-जैसे शक्ति का आरोहण होता है मूलाधार से लेकर सहस्रार तक वैसे-वैसे शिव का साक्षात्कार होता है। शक्ति का यह आरोहण कुण्डलिनी है और शिव का वह निवास शून्य, वह सहस्रार है, वह परम शान्ति की भूमि, वहीं समाधि है, जहाँ साधक और ब्रह्म, शक्ति और शिव, अनुभव और अनुभूति एक हो जाते हैं। शिव और शक्ति की एकता केवल किसी तांत्रिक या योगी का रहस्य नहीं है; यह भारतीय जीवनदर्शन का मूलाधार है।
गृहस्थ से लेकर सन्यासी तक, भक्त से लेकर दार्शनिक तक, सभी को यह स्वीकार करना होता है कि ब्रह्मांड की रचना किसी एक तत्त्व से नहीं हुई, बल्कि दो तत्त्वों की लयात्मक संधि से हुई है जो कि चेतना और क्रिया, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति है। यह संधि यदि टूटती है, तो सृष्टि का ताना-बाना ही बिखर जाता है।
हम देखते हैं कि भारतीय नारी की आदर्श छवि शक्ति के रूप में ही प्रतिष्ठित है। वह आत्मा की सामर्थ्य है जिसे शिव ने अर्धनारीश्वर रूप में इस एकता को शरीर पर अंकित कर दिया; आधा पुरुष, आधा स्त्री; आधा शान्ति, आधा गति; आधा निर्गुण, आधा सगुण। यह अद्भुत समन्वय उस तत्वमीमांसा का प्रतीक है जो हमें यह बताता है कि जब तक चेतना और शक्ति एक नहीं होती, तब तक जीवन अपूर्ण रहता है और जब यह एकता साकार होती है, तभी जीवन, मोक्ष और परमानन्द की पूर्णता संभव है।
अंततः, यही कहा जा सकता है कि शिव और शक्ति की यह दार्शनिक एकता भारतीय चिन्तन की वह धुरी है, जिस पर समस्त धर्म, योग, साधना, कला, संस्कृति और नैतिकता का महान भवन निर्मित है। इस एकता को जो जानता है, वह द्वैत और अद्वैत दोनों को पार कर चुका होता है। वह शिव है, वह मुक्त है, वही परब्रह्म है।
(लेखक विकास मिश्र महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के शोधार्थी हैं और ये उनके निजी विचार हैं)
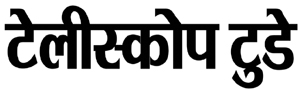 Telescope Today | टेलीस्कोप टुडे Latest News & Information Portal
Telescope Today | टेलीस्कोप टुडे Latest News & Information Portal



