शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो, मानव को पूर्ण मानव बनाती है। हमारी नई शिक्षा नीति- 2020 भी शिक्षा को पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने ‘एक न्याय संगत और न्याय पूर्ण समाज के विकास और राष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है।’ ऐसा मानती है। मानव के लिए शिक्षा जहां एक मूलभूत आवश्यकता है, वहां कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा के मार्ग में अवरोध की भांति चल रहे परिषदीय विद्यालयों (छात्र संख्या 50 से कम) के मर्जर का मर्ज नौनिहालों को आहत कर रहा है।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून 2025 को जारी एक आदेश के क्रम के अनुपालन में 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को निकटतम 500 मीटर दूरी वाले विद्यालय में विलय किया जा रहा है तथा 100 एवं 150 छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक पद समाप्त किया जा रहा है।
हाई कोर्ट से मर्जर याचिका के खारिज होने पर सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली। बहुविध विरोधों को दरकिनार करते हुए 10827 विद्यालयों का विलय प्रदेश भर में किया गया। विभाग का कहना है या कहें कि, विलय की विशेषताएं गिनाई जा रही हैं, कि इससे छात्रों को विशेष बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सकेगा। आधारभूत ढांचे और भी मजबूती पा सकेंगे। स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं बेहतर मिल सकेंगे। जैसे बच्चा घर से इतनी दूर विद्यालय आता है, वहीं वह 500 मी. ही तो दूर जा रहा है कौन सा उसे घर से कई किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। इसमें अभिभावकों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किंतु, संकेत कहता है कि सरकार निजीकरण की ओर कदम बढ़ा चुकी है उसका क्या? विद्यालय मर्ज किए जाएंगे इससे अधिक लाभ किसे है? स्पष्ट है। हानि किसे है? हम गिना सकते हैं -दलित, पिछड़े, मजदूर वर्ग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि, वह अपने बच्चों के लिए स्कूल वैन, महंगे स्कूल, महंगी किताबें -कॉपियां, सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कर पाते इसलिए वे अपने बच्चों को नजदीक के सरकारी विद्यालयों में भेजते हैं। जहां उन्हें नि:शुल्क शिक्षा और नि:शुल्क भोजन दिया जाता है।
बुनियादी शिक्षा का आधार भी यही है कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क अबाध शिक्षा की व्यवस्था करें। राइट टू एजुकेशन- 2009 जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानकों का निर्धारण किया गया। शिक्षा तक पहुंच और उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई। विद्यालयों को मर्ज किए जाने से शिक्षा तक पहुंच में बाधा उत्पन्न तो हो ही रही है साथ ही मर्ज किए गए विद्यालयों में उपस्थित भी प्रभावित हो रही है।
शिक्षक का कार्य है शिक्षित करना वह तो अपना कार्य करता रहेगा। वह जहां भी भेजा जाएगा वहां अपना कार्य उसी निष्ठा से करेगा। मर्जर से उसके हित -अहित को थोड़ी देर के लिए अलग रखने पर अहित किसका नजर आ रहा है? उन दलित, पिछड़े, कमजोर वर्गों का, जो भावनात्मक रूप से 5 वर्षों के लिए अपने निकटतम सरकारी विद्यालयों से जुड़ चुका है।
अब कुछ प्रश्न और विचार जो बार-बार उभर रहे हैं। कि, जिन विद्यालयों को अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में मर्ज कर दिया गया है। उन विद्यालय भवनों में अब आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे। यह कार्य बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा तेजी से शुरू किया जा रहा है। कम छात्र संख्या के कारण विद्यालय मर्ज किया गया, क्या इस विद्यालय में आंगनबाड़ी को सम्बद्ध रूप से संचालित नहीं किया जा सकता था? आंगनबाड़ी के बाद प्रथम कक्षा के लिए बच्चा वहीं से मिल जाता उसे अन्यत्र नहीं जाना होता। क्या यही स्थिति आगे आँगनवाड़ी केंद्रों के लिए नहीं आएगी?
परिषदीय विद्यालयों को कायाकल्प के अन्तर्गत 19 पैरामीटर से संतृप्त किया जा रहा है। प्रदेश भर के विद्यालयों पर करोड़ों रूपये ख़र्च किये गए। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों पर इतना खर्च करते समय दूरदर्शिता का परिचय क्यों नहीं मिला? इस कोष का उपयोग कैसे किया जा सकता था..? जिन विद्यालयों की छात्र संख्या पिछले 5 सालों से निरंतर कम हो रही थी उन्हें भी वही सुविधा प्रदान की गई जो निरंतर छात्र संख्या में वृद्धि कर रहे थे। तराजू से तौलते समय दोनों पलड़ों में मात्रा समान होती है, वस्तु समान नहीं होता।
कुछ विद्यालयों को यदि छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे परिषदीय विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालयों के सुविधाओं को भी मात दे सकते हैं। ऐसे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहालों की भावनाएं, उनका रोना, बिलखना और बीच में ही छोड़ कर चले जाने की विवशता और कुछ की पढ़ाई पर असर पड़ जाना। यह क्या कचोटता नहीं है?चलिए, इधर ध्यान नहीं भी दिया जाए तो क्या घटती छात्र संख्या के जिम्मेदार शिक्षक वर्ग ही हैं? नहीं। यह हम भी जानते हैं शिक्षक ने हमेशा से प्रशासन के साथ मिलकर ही कार्य किया है। उसके आदेशों को शिरोधार्य किया है।
शिक्षक साधारण नहीं होता है। यह सब जानते हैं।सरकार की मंशा इस विषय में न्याय योग्य नहीं लगती। कम छात्र संख्या लगभग 10 या 5 रह जाने पर यदि निकटतम विद्यालय में मर्ज कर दिया जाए तो कष्ट संभवतः कम हो।किंतु, जिन विद्यालयों की छात्र संख्या 10 है उन्हें भी और जो 50 से कम अर्थात 49 या 48 हैं उन्हें भी मर्ज किया जा रहा है। यह बहुत कष्टकारी है। क्या विलय ही इसका विकल्प है? इसकी क्या प्रत्याभूति (गारंटी) है कि, जिन विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है उनकी छात्र संख्या निरंतर बढ़ेगी या शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी ही?
सरप्लस होते हेड मास्टर को देखते हुए क्या यह समझने की भूल हम कर सकते हैं? कि, आगे भविष्य में भावी शिक्षकों के मार्ग अवरुद्ध नहीं किए जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से प्रमोशन के लिए आस लगाए बैठे शिक्षक पद गँवाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। जिसका कारण घटती छात्र संख्या है। ऐसे शिक्षक जो माध्यमिक की योग्यता रखते हैं।उन्हें कोई एक परीक्षा लेकर वहां भी भेजा जा सकता था। किंतु,ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
शिक्षक विवश होते जा रहे हैं। सरकार या विभाग की मंशा अनुरूप कार्य करना एक अलग बात है। किंतु शिक्षक होने के नाते अपनी बात रखना भी आवश्यक है। विद्यालय मर्जर हेतु सहमति -असहमति को किनारे करते हुए जिस प्रकार बाध्यकारी नीतियां अपनाई जा रही है वह न्याय संगत नहीं है। विद्यालय में smc भंग हो जाने, विद्यालय की पंजिकाओं, फर्नीचर, व्यवस्था, साज -सज्जा आदि आकर्षण अन्य को किनारे करते हुए परिषदीय विद्यालयों को यह कहते हुए मर्ज करना कि, इससे शैक्षिक गुणवत्तापूर्ण स्थितियां सुधरेंगी। यह संदेहास्पद लगता है।
घटती छात्र संख्या चिंता का विषय है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए पुनः अभियान चलाकर प्रयास किया जा सकता है। किंतु, समस्या के समुचित समाधान की ओर ध्यान आकृष्ट कराना भी आवश्यक है। विलयरूपी विकल्प में किसी नौनिहाल के सपने विगलित न हो यह ज्यादा आवश्यक है।

(लेखिका डॉ. संगीता प्राथमिक विद्यालय दामोदरपुर बंकी-बाराबंकी की प्रधानाध्यापिका हैं और ये उनके निजी विचार हैं)
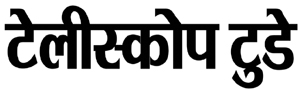 Telescope Today | टेलीस्कोप टुडे Latest News & Information Portal
Telescope Today | टेलीस्कोप टुडे Latest News & Information Portal



