डॉ. एस. के. गोपाल
जहाँ आज उत्तर प्रदेश का भव्य विधान भवन स्वाभिमान से खड़ा है, कभी वहाँ एक खुला मैदान हुआ करता था। अंग्रेजी शासन के समय तक इलाहाबाद ही प्रदेश की राजधानी थी और समस्त प्रशासनिक कार्य वहीं से संचालित होते थे। परंतु जैसे-जैसे अंग्रेजों का विस्तार बढ़ता गया, उन्हें अधिक स्थान और सुविधाओं की आवश्यकताएँ महसूस हुईं। लखनऊ अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामरिक विशेषताओं के कारण अंग्रेजों का पसंदीदा नगर था। परिणामस्वरूप 1922 में लखनऊ को राजधानी घोषित किया गया और उसी वर्ष दिसंबर में काउंसिल हाउस (वर्तमान विधान भवन) का निर्माण आरम्भ हुआ, जो लगभग सात वर्ष में पूर्ण हुआ।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा 20 मई 1952 को गठित हुई। तब से अब तक 17 विधानसभाएँ अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं और वर्तमान 18वीं विधानसभा का कार्यकाल अन्तिम वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। राज्य की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसी भवन से संचालित होती है। यहाँ 403 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा एक नामित सदस्य जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार उच्च सदन विधान परिषद में विविध क्षेत्रों से चुनकर आए तथा मनोनीत कुल सौ सदस्य महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं। दोनों सदनों में विधेयकों पर विचार होता है, नीतियाँ बनती हैं और शासन-प्रशासन की दिशा तय होती है।
अट्ठारहवीं विधानसभा में विधानमंडल की नियमावली संशोधित कर उसे नए स्वरूप में प्रख्यापित भी किया गया है। परंतु पिछले लगभग दो दशक में एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभरकर सामने आई है, सत्ता पक्ष द्वारा विधायी परंपराओं और मूल्यों की अवहेलना। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है डिप्टी स्पीकर का पद, जो परंपरागत रूप से विपक्ष को मिलता रहा है। किंतु बसपा, सपा और अब भाजपा, तीनों ही दलों ने सत्ता में रहते हुए इस पद को लम्बी अवधि तक रिक्त रखा। सत्रहवीं विधानसभा के अंतिम वर्ष में नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर अवश्य बनाया गया, परंतु तब वह अपनी राजनीतिक निष्ठा को लेकर विवादों में रहे और बाद के वर्षों में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते और सरकार में मंत्री भी बने।
आज स्थिति यह है कि विधान सभा की अनेक महत्वपूर्ण समितियाँ- याचिका समिति, लोक लेखा समिति, प्रतिनिहित विधायन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, तथा स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच संबंधी समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति आदि के कार्य संतोषप्रद नहीं कहे जा सकते। जिन समितियों का उद्देश्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना था, वे अब लगभग दंतहीन और निष्प्रभावी सी होकर रह गई हैं। उनके कामकाज का दायरा केवल औपचारिकताओं की पूर्ति तक सिमट गया है।
यह स्थिति तब और अधिक चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष तथा संसदीय कार्य मंत्री, दोनों ही विधायी विषयों के अत्यंत अनुभवी, सरल और निस्पृह व्यक्तित्व वाले नेता हैं। फिर भी क्यों डिप्टी स्पीकर जैसा संवैधानिक पद रिक्त है? समितियों की कार्यवाही मात्र खानापूर्ति बनकर क्यों रह गई है? सदस्यों के विशेषाधिकार मामलों की सुनवाई वर्षों तक लटकी रहे तो जनता के हितों की आवाज़ आखिर किस तरह प्रभावी मानी जाए?
वर्तमान परिस्थितियाँ संकेत देती हैं कि यदि विधायी मूल्यों और संसदीय परंपराओं को शीघ्र ही संरक्षण नहीं मिला, तो लोकतांत्रिक ढाँचे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आवश्यक है कि सभी दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन की गरिमा, परंपराओं और मर्यादा के संरक्षण का संकल्प लें। समितियों की कार्यवाही सशक्त और पारदर्शी हो, तथा जनता से जुड़े मुद्दों पर निष्पक्ष और गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श सुनिश्चित किया जाए। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब विधानमंडल प्रभावी, सक्रिय और जिम्मेदार हो। इसलिए विधायी मूल्यों का संरक्षण आज समय की सबसे महत्वपूर्ण मांग है।
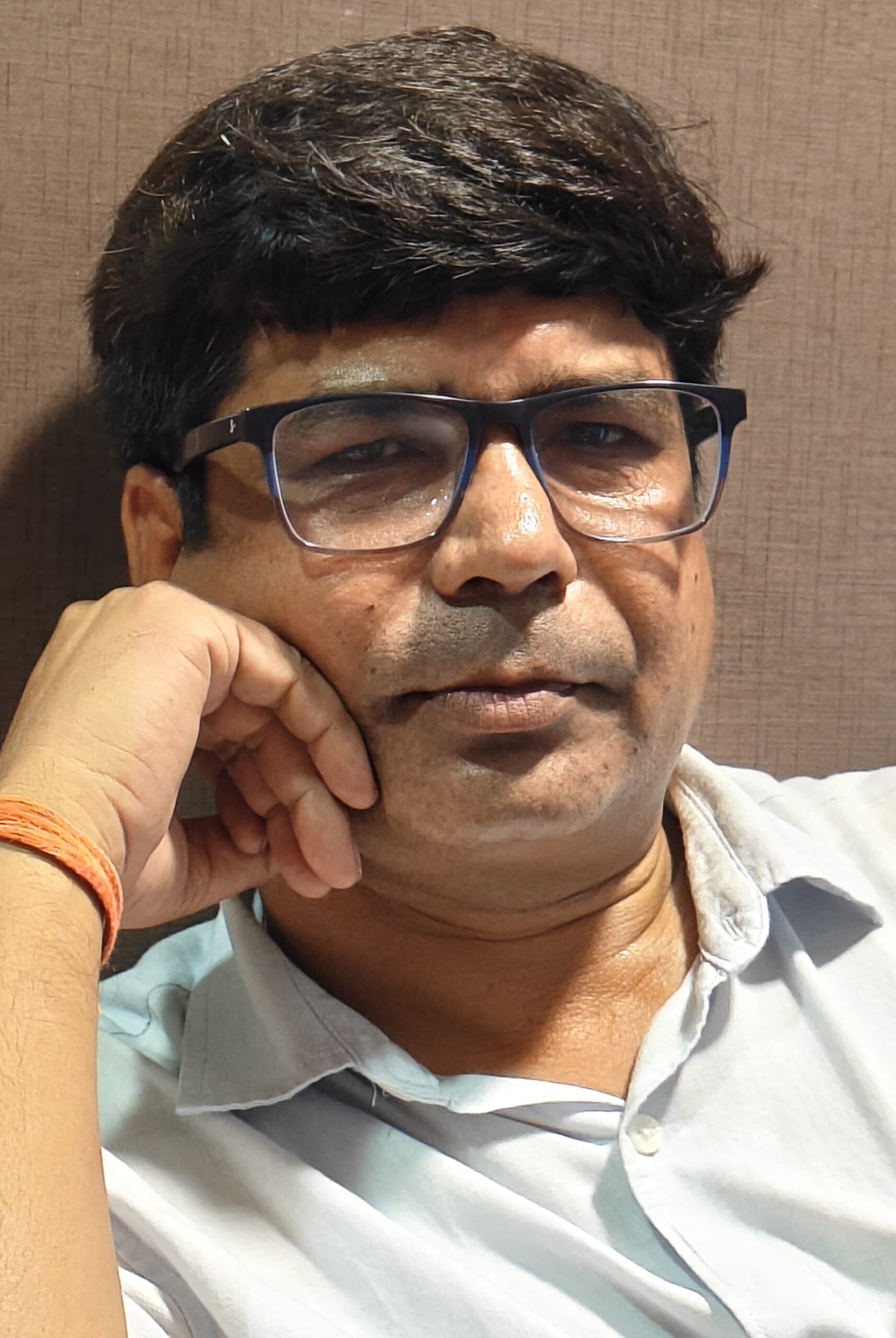
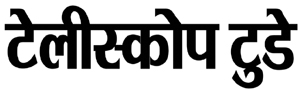 Telescope Today | टेलीस्कोप टुडे Latest News & Information Portal
Telescope Today | टेलीस्कोप टुडे Latest News & Information Portal



