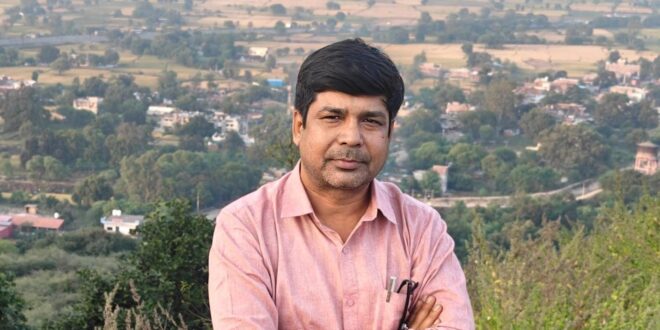डॉ. एस. के. गोपाल
भारतीय जीवन में विवाह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उस सांस्कृतिक श्रृंखला का केंद्रीय संस्कार है, जिसकी डोर पीढ़ियों से चली आ रही है। विवाह का अर्थ मात्र दो व्यक्तियों का साथ आना नहीं, बल्कि दो कुलों, दो परिवारों और दो आत्माओं का ऐसा मिलन है, जो उन्हें गृहस्थाश्रम की पवित्र नींव पर स्थापित करता है। इस बंधन में केवल प्रेम या सामाजिक मान्यता नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और आध्यात्मिक उत्कर्ष की वह चेतना समाहित है, जिसे हमारे पूर्वजों ने इक्कीस पीढ़ियों तक मुक्ति और सात जन्मों का साथ जैसी दिव्य कल्पनाओं से जोड़ा है। यह सुख-संगति का आधार नहीं, बल्कि मोक्ष की यात्रा का सहचर भी माना जाता है। परंतु समय की धारा जब नई दिशाओं में मुड़ती है तो संस्कार भी उसके प्रभाव से अछूते नहीं रहते। पिछले कुछ वर्षों में विवाह संस्कार पर बाजारीकरण की लहर जिस तरह से छाई है उसने इसके सहज, आत्मीय और सांस्कृतिक स्वरूप को धीरे-धीरे नया रूप दे दिया है। लोकगीतों का मधुर कंपन, परिवार की सरल भागीदारी और घर-आँगन में गूँजता उल्लास जैसे पीछे छूटते जा रहे हों और उनकी जगह सजावटी मंच, नृत्य-नाटिका और कृत्रिम रोशनी ने ले ली हो।
हल्दी चढ़ाने जैसी आत्मीय रस्में, जहाँ कभी घर की वधुएँ, देवर-भाभी और ननदें हँसी-ठिठोली में सारे आँगन को पीला कर देती थीं, अब पीले परिधानों, थीम फोटोग्राफी और मेहमानों के लिए विशेष कार्यक्रम के रूप में सामने आती हैं। रस्म तो वही है पर उसकी आत्मा कुछ कम महसूस होती है। मंगल गीतों का स्वर जो विवाह की संपूर्ण प्रक्रिया में आशीर्वाद का रूप लेकर बहता था अब भी कहीं-कहीं सुनाई देता है लेकिन अधिकांश जगह वह डीजे के शोर में दब चुका है। गीतों की जगह बास की थरथराहट और संगीतमय मंगल कामनाओं की जगह जोरदार लय, यह परिवर्तन सिर्फ श्रवण का नहीं, संस्कार के स्वर का भी है। विवाह का सरल जयमाल प्रसंग, जो कभी दो हृदयों की प्रथम मिलन-रश्म माना जाता था, अब रंग-बिरंगी रोशनी, ऊँचे मंच, गुलाब वर्षा और धुएँ के झरनों का प्रदर्शन बन गया है। वर-वधू के लिए यह आनंद का क्षण अवश्य है किंतु इसके पीछे खड़ी तमाशाई नाटकीयता कई बार विवाह की सहज गरिमा को अदृश्य कर देती है। कई पुरोहित इस क्षरण पर चिंता भी जताते हैं, पर यजमानों की इच्छा और आयोजनकर्ताओं की भव्यता के सामने उनकी आह मात्र औपचारिक रह जाती है।
कोरोना काल ने विवाह संस्कृति को अप्रत्याशित रूप से नए अर्थों में पुनर्परिभाषित किया। महामारी के दिनों में जब बड़े आयोजन संभव नहीं थे, अनेक परिवारों ने अत्यंत सीमित उपस्थिति में सादगीपूर्ण विवाह सम्पन्न किए। केवल परिजन, कुछ थोड़े रिश्तेदार और आवश्यक कर्मकांड, इन्हीं के बीच विवाहों की वह आत्मीयता पुनर्जीवित हुई, जो लंबे समय से चमक-दमक में कहीं खोती जा रही थी। कई लोगों ने पाया कि कम भीड़, कम तामझाम और सीमित व्यवस्था में विवाह कहीं अधिक शांत, स्वाभाविक और भावनात्मक होता है। इसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए कुछ परिवार अब भी विवाह को पारिवारिक घेरे में सम्पन्न कर लेते हैं और बाद में केवल आशीर्वाद समारोह के रूप में प्रीतिभोज रखते हैं। इससे जहाँ खर्च का बोझ कम होता है, वहीं रस्मों की गंभीरता और आत्मा भी अक्षुण्ण रहती है। विवाह संस्कार का अर्थ यदि केवल भौतिक सज्जा, प्रदर्शन या सामाजिक प्रतिस्पर्धा तक सीमित रह जाए तो यह न केवल परम्पराओं का अपमान है, बल्कि संस्कार का मूल्यह्रास भी है। विवाह अपने मूल में उत्सव अवश्य है पर यह उत्सव गहराई में उतरकर मनुष्य को संयम, मर्यादा और जिम्मेदारी का बोध कराता है। नवाचारों का स्वागत है, लेकिन ऐसे नवाचार जो दिखावे, फिजूलखर्ची और कृत्रिमता के रूप में सामने आते हैं, वे संस्कार को कमजोर करते हैं, उसका विस्तार नहीं।
समय बदलता है और उसके साथ रस्मों का स्वरूप भी। परंतु परिवर्तन का अर्थ मूल मूल्य को त्यागना नहीं होता। विवाह सदियों से हमारे समाज की आत्मा रही है, एक ऐसा संस्कार जिसके कारण परिवार स्थिर रहते हैं, समाज की संरचना सुव्यवस्थित रहती है और मनुष्य अपने जीवन की दिशा को परिपूर्णता की ओर मोड़ता है। अतः समाज के लिए यही उपयुक्त होगा कि वह विवाह को आधुनिकता और परम्परा के बीच संतुलित रूप में देखे, जहाँ नई परम्पराएँ जुड़ें पर पुरानी परम्पराओं की गरिमा न टूटे; जहाँ सौंदर्य हो, पर दिखावा न हो; जहाँ आयोजन हो, पर संस्कार न बिखरे। विवाह अंततः दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों का, दो परंपराओं का, और दो जीवनदृष्टियों का मिलन है। इसे इवेंट बनाने के बजाय अनुभव बनाना ही इसकी सबसे सुंदर परिणति है। यही इसकी संस्कृति है और यही इसकी शाश्वत गरिमा भी।
(लेखक डॉ. एस. के. गोपाल समाजशास्त्री और स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके निजी विचार है)
 Telescope Today | टेलीस्कोप टुडे Latest News & Information Portal
Telescope Today | टेलीस्कोप टुडे Latest News & Information Portal